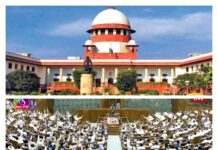शिक्षा का उद्देश्य विवेकानंद जी के अनुसार बालक के अंदर निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। विद्यालय में बालक जो भी ज्ञान प्राप्त करता है उससे अपने जीवन के उद्देश्य निर्धारित करता है। किसी भी बालक के जीवन के उद्देश्य स्वयं की पहचान और आजीविका प्राप्त करने से अधिक नहीं होते। बहुत कम प्रतिशत बालक मानव और मानवता की सेवा, उत्थान और उनके जीवन की श्रेष्ठता का कार्य करते हैं। स्वयं का उत्थान करना भी इसी के अंतर्गत आता है। यदि प्रत्येक बालक शिक्षा के माध्यम से स्वयं का विकास करता है, आजीविका तलाशता है तो किसी और को किसी और के लिए कुछ करने की आवश्यकता शायद ही रह जाये।
वर्तमान विद्यालयी शिक्षा व्यवहारिक होने के स्थान पर सैदांतिक एवं अव्यवहारिक है। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत यदि किसी छात्र की व्यावसायिक दक्षता या अन्य किसी भी कार्य में निपुणता देखी जाए तो वह शून्य होती है। पंद्रह वर्ष की शिक्षा के उपरांत यदि छात्र स्वयं की आजीविका का प्रबंध करने में असमर्थ है तो विद्यालयी शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

इस परिवर्तन को यदि बिन्दुवार देखें तो मैं विद्यालयी शिक्षा में अग्रांकित सुधार की माँग करना चाहूंगा-
1. विद्यार्थियों को अध्यनशील बनाते हुए उन्हें अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
2. विद्यार्थियों की शिक्षा को अंकपत्र तक सीमित न करके उन्हें स्वयं के जीवन को सार्थक अर्थों में अन्वेषित करने योग्य बनाये।
3. पाठ्यक्रम में पूर्ण सैदांतिक विषयवस्तु के स्थान पर उसके व्यवहारिक प्रयोग की विषय-वस्तु को सम्मिलित करना चाहिए, यदि व्यवहारिक विषय-वस्तु उपलब्ध नहीं है तो शिक्षा के विकास और उन्नयन के नाम पर ‘सौं दिन चले अढ़ाई कोस’ संस्थाओं की जवाबदेही तय करते हुए सार्थक परिणामों पर जोर देना चाहिए।
4. विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को उनकी आवश्यकता के अनुरूप संवर्द्धित करना चाहिए।
5. जीवन के लिए सम-विषम परिस्थितियों का आंकलन करते हुए विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम आवश्यक दक्षताओं को सुनिश्चित करना चाहिए एवं छात्रों को ऐसी परियोजनाओं को बनाकर देनी चाहिए जिन्हें पूर्ण करते हुए वे जीवन के लिए आवश्यक उन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें।
6. सरकार के विभिन्न विभागों को भी विद्यालयी शिक्षा से जोड़ना चाहिए ताकि छात्र वहाँ की कार्यप्रणाली समझ सके। इससे भृष्टाचार में भी लगाम लगेगी। बहुत सारे विभाग एक अबूझ पहेली होते है, जहाँ काम कराने के लिए यही विद्यार्थी, देश के भावी भविष्य भृष्टाचार का शिकार होते है। समझ होने पर सहज ही इस पर लगाम लगेगी।
7. देश के तमाम शिक्षाविदों ने तमाम समितियों में तरह-तरह की सुधार की बातें बतायी। उनके लागू होने में लगने वाला समय अन्य विविध समस्याओं को जन्म देता है। जिनके निदान के लिए पुनः नयी समिति गठित होती है। और फिर लम्बा समय। ऐसे में समिति की सिफारिशों पर त्वरित गति से कार्यवाही होते हुए शिक्षा के क्षेत्रों में लागू करना चाहिए।
8. विद्यार्थियों के अन्दर आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनने के गुण को विकसित करने के साथ-साथ उस गुण के पुष्पित-पल्लवित होने के वातावरण का निर्माण भी होना चाहिए।
9. समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का निराकरण छात्र आयोजित प्रतियोगिताओं में अपने विचारों के माध्यम से देते हैं। प्रतियोगिता के उपरांत उस पर भी ठोस कार्य होना चाहिए। सिर्फ ताली बजाकर, पदक देकर और प्रमाण पत्र देकर इतिश्री करने से बचना चाहिए।
10. माता-पिता और रिश्तेदारों की अपेक्षाओं से बचाकर विद्यार्थियों की क्षमता और योग्यता का वास्तविक आँकलन करना और उस आँकलन को उन्हें स्वीकार करने तथा उद्देश्यों के अनुरूप संघर्ष हेतु मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना।
“हकीकत-ए-अफसाना जो है, उस पर गौर फरमाएँ।
गर्त में जा रहे भविष्य को सप्रयास बचाएं।।
ढल रहा देश का भविष्य इन कक्षाओं में।
इनके लिए वास्तविक और सुन्दर माहौल बनाएं।।”
( लेखक- प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव, स्नातकोतर शिक्षक (संगणक )- विज्ञान, केंद्रीय विद्यालय न्यू बंगाईगाँव हैं ।)